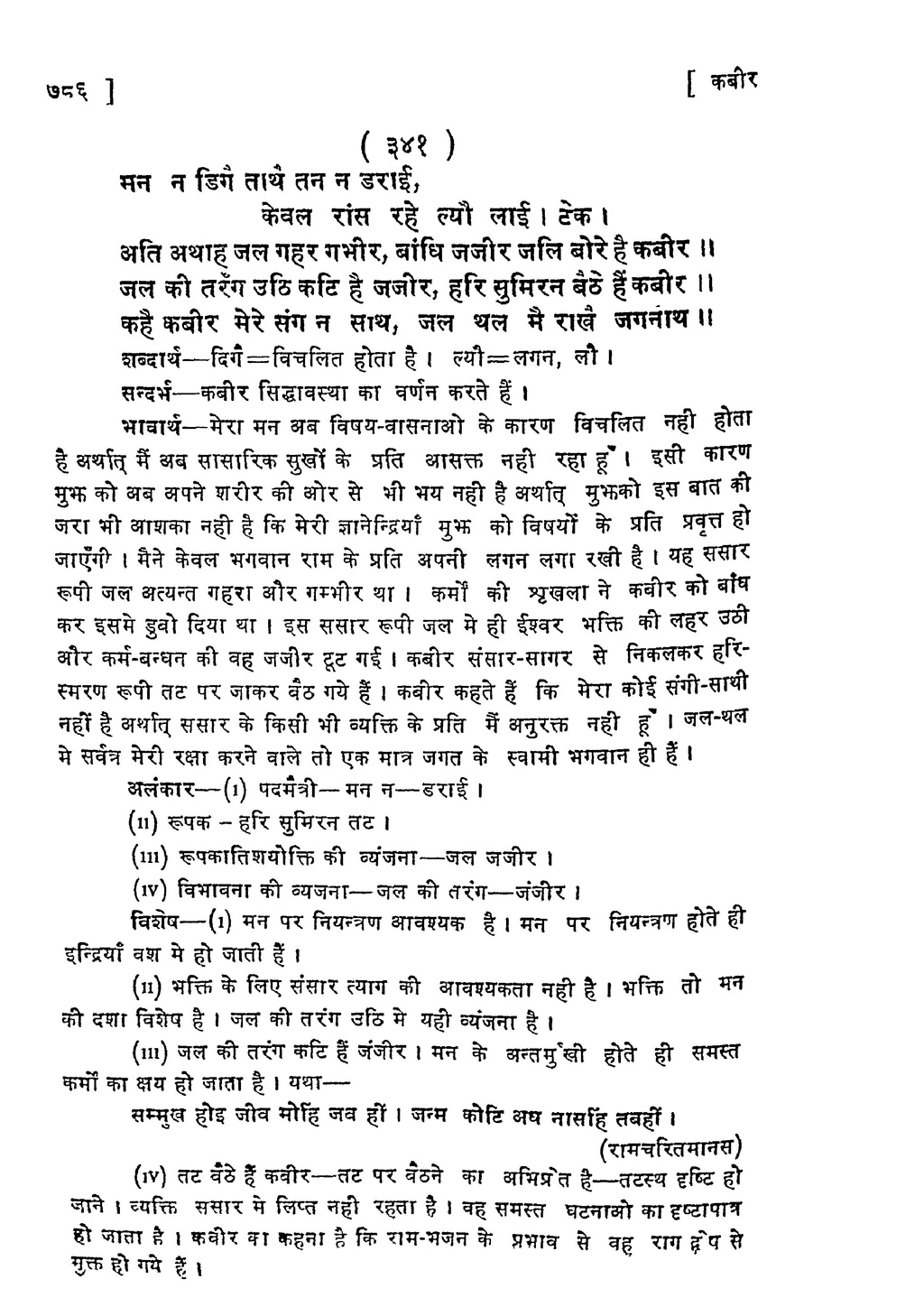(३४१)
मन न डिगै ताथै तन न डराई,
केवल रांस रहे ल्यौ लाई। टेक।
अति अथाह जल गहर गभीर, बांधि जजीर जलि बोरे है कबीर॥
जल की तरँग उठि कटि है जजीर, हरि सुमिरन बैठे हैं कबीर॥
कहै कबीर मेरे संग न साथ, जल थल मै राखै जगनाथ॥
शब्दार्थ—दिगै=विचलित होता है। ल्यौ=लगन, लौ।
सन्दर्भ—कबीर सिद्धावस्था का वर्णन करते हैं।
भावार्थ—मेरा मन अब विषय-वासनाओ के कारण विचलित नही होता है अर्थात् मैं अब सासारिक सुखों के प्रति आसक्त नही रहा हूँ। इसी कारण मुझ को अब अपने शरीर की ओर से भी भय नही है अर्थात् मुझको इस बात की जरा भी आशका नही है कि मेरी ज्ञानेन्द्रियाँ मुझ को विषयों के प्रति प्रवृत्त हो जाएँगी। मैने केवल भगवान राम के प्रति अपनी लगन लगा रखी है। यह ससार रूपी जल अत्यन्त गहरा और गम्भीर था। कर्मों की श्रृंखला ने कबीर को बाँध कर इसमे डुबो दिया था। इस ससार रूपी जल मे ही ईश्वर भक्ति की लहर और कर्म-बन्धन की वह जजीर टूट गई। कबीर संसार-सागर से निकलकर हरि-स्मरण रूपी तट पर जाकर बैठ गये हैं। कबीर कहते हैं कि मेरा कोई संगी-साथी नहीं है अर्थात् ससार के किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं अनुरक्त नही हूँ। जल-थल मे सर्वत्र मेरी रक्षा करने वाले तो एक मात्र जगत के स्वामी भगवान ही हैं।
- अलंकार—(i) पदमैत्री—मन न—डराई।
- (ii) रूपक—हरि सुमिरन तत।
- (iii) रूपकातिशयोक्ति की व्यंजना—जल जजीर।
- (iv) विभावना की व्यजना—जल की तरंग—जंजीर।
विशेष—(i) मन पर नियन्त्रण आवश्यक है। मन पर नियन्त्रण होते ही इन्द्रियाँ वश मे हो जाती हैं।
(ii) भक्ति के लिए संसार त्याग की आवश्यकता नही है। भक्ति तो मन की दशा विशेष है। जल की तरंग उठि में यही व्यंजना है।
(iii) जल की तरंग कटि हैं जंजीर। मन के अन्तर्मुखी होते ही समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। यथा—
सम्मुख होइ जीव मोहि जब हीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं।
(रामचरितमानस)
(iv) तट बैठे हैं कबीर—तट पर बैठने का अभिप्रेत है—तटस्थ दृष्टि हो जाने। व्यक्ति ससार मे लिप्त नही रहता है। वह समस्त घटनाओ का दृष्टापात्र हो जाता है। कबीर का कहना है कि राम-भजन के प्रभाव से वह राग द्वेष से मुक्त हो गये हैं।